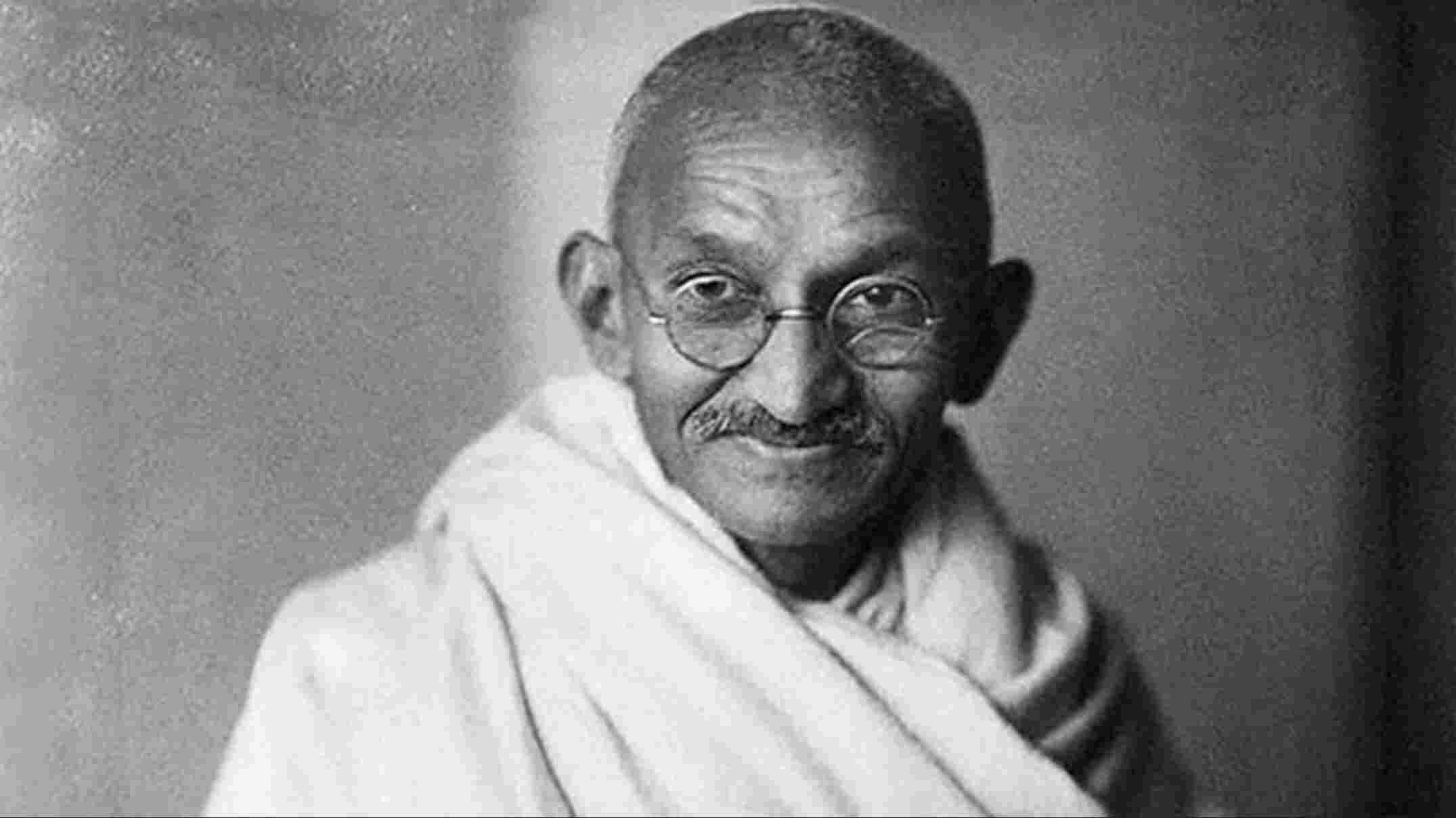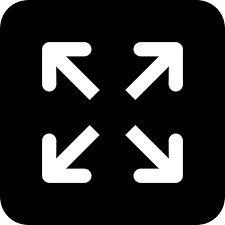यूपी सरकार के छोटे से बदलाव के कारण सोनभद्र, चंदौली जिले की धंगड़ जाति को अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र मिलना हो गया बंद (फोटो : प्रतीकात्मक)
पिछले बीस वर्षों में हिंदी के जिन कहानीकारों ने अपनी अलग एवं विशिष्ट बनाई है उनमें मनीषा कुलश्रेष्ठ सबसे अधिक लोकप्रिय और सम्मानित रचनाकार हैं। वह अपने शिल्प, भाषा और कथ्य के बीच एक परिपक्व संतुलन बनाकर चलती हैं। उनकी कहानियों में पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करने की अद्भुत रवानगी है और तनिक भी विषयांतर नहीं है। वह एक सचेत कथालेखिका हैं और उनके स्त्री विमर्श में सामाजिक ताने—बाने पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करने का साहस भी संवेदना, आवेग और तर्कों के साथ है। यहां दी जा रही उनकी कहानी 14 साल पहले वागर्थ में छपी थी और आदिवासी लड़कियों के यौन शोषण की हिंदी में संभवतः पहली कहानी थी। तब मीडिया में उतनी प्रमुखता से यौन शोषण का मुद्दा नहीं उठा था जितना आज me too आंदोलन के बाद से उठा है। जो लोग इस आंदोलन को केवल मध्यवर्गीय शहरी महिलाओं तक सीमित कर उसे नकार देना चाहते हैं उन्हें मनीषा की यह कहानी जरूर पढ़नी चाहिए।कहानीकार ने इस ट्रामा को बहुत सूक्ष्म ढंग से पेश किया है। मनीषा कुलश्रेष्ठ कहानीकार के अलावा कुशल नृत्यांगना, उपन्यासकार और कवि भी हैं। हाल ही में बिरजू महाराज पर उनकी एक पुस्तक भी आई है। आइए पढ़ते हैं मनीषा कुलश्रेष्ठ की कहानी 'अवक्षेप'—विमल कुमार, वरिष्ठ पत्रकार और कवि
अवक्षेप
 मनीषा कुलश्रेष्ठ
मनीषा कुलश्रेष्ठ
कहानी लिखना क्या आसान काम है?
रवीन्द्रनाथ टैगौर के अनुसार 'रचना का जन्म लेना और प्रसवपीड़ा एक समान है।' मेरे लिये तो यह और भी दुश्कर है। मेरे लिये कहानी लिखना स्वयं जन्म लेता हुआ शिशु होना है। अनजाने फिसलन भरे रास्तों पर‚ अनजाने दबावों और खींचतान के बीच अजनबी जगह पर‚ अनजाने ठण्डे हाथों में उतर आना है‚ कहानी लिखना। कम से कम इस बार तो यही महसूस हुआ है। स्वानुभूत कहानी हो तो… कहानी लिखना‚ सूखते खुरंटों को उखाड़–उखाड़ कर हरा करना है। कल्पना या फंतासी हो तो… कहानी लिखना अवचेतन की गुह्य‚ अनदेखी गलियों से गुज़रना है। कहानी लिखना‚ कोकून में कैद कीड़े का‚ अपनी ही बनाई कैद से तमाम जद्दोजहद के बाद बाहर निकलना है। मुझे नहीं पता यह कहानी कल्पना है या सत्य? फंतासी है या अर्धसत्य? मेरे जीवन से उलझ कर‚ गुज़र गई कोई घटना है या मन पर पड़ा कोई अतीत का निशान! मुझे सच में नहीं पता। जब से इसे लिखना शुरु किया तबसे मैं सोते–जागते इसी कहानी की प्रेतबाधा से ग्रसित हूँ। इसे लिखते–लिखते मैं स्वयं इन्सोम्निया का शिकार हो गई हूँं‚ पूरे हफ्ते से सोई कहां हूं? अजीबो–गरीब सपनों के बीच–बीच में से पसीना–पसीना हो कर कई बार मध्यरात्रि में उठ बैठी हूँ। यकीन मानिये अब इस कहानी के आदि–अंत पर भी मेरा अधिकार नहीं रहा है। मुझे नहीं पता अंत होते–होते यह कहानी कहां पहुंचने वाली है। कहानी लिखने के पहले ही दिन की तो बात है‚ मैंने उस रात सपने में देखा-
शहर के बीचोंबीच‚ एक रेज़ीडेन्सी कैम्पस है। इतिहास कहता है‚ पहले यहां अंग्रेजों की रेज़ीडेन्सी थी‚ पर अब इस रेज़ीडेन्सी के पेड़ों से भरे विस्तृत क्षेत्र और इमारतों में एक कन्या महाविद्यालय‚ उसका हॉस्टल‚ एक सीनियर सैकेण्ड्री गर्ल्स स्कूल‚ एक एसटीसी गर्ल्स स्कूल और उनका छात्रावास‚ एक मेडिकल कॉलेज का पीजी गर्ल्स हॉस्टल है‚ एक उजाड़ कोने में आदिवासी कन्या छात्रावास भी है। इनमें से कुछ इमारतें नई हैं‚ कुछ पुरानी ऐतिहासिक इमारतों को बढ़ा–घटा कर स्कूल–कॉलेज लायक बना लिया गया है। इस रेज़ीडेन्सी के तीन गेट हैं। एक कन्या महाविद्यालय का मेन गेट है‚ जो बाकि शहर की बढ़िया मुख्य सड़कों से जुड़ा है। एक कन्या महाविद्यालय को हॉस्टल से जोड़ती सड़क है‚ उसके बीच से काट कर एक सड़क रेज़ीडेन्सी सीनियर सैकेण्ड्री स्कूल को जाती है… तो उसके उस तरफ स्कूल की निकासी का एक बड़ा गेट है‚ उसके बाहर पुलिस चौकी है। पुलिस चौकी के बाहर निकल कर चेतक सर्कल है‚ जहां शहर के पिक्चर हॉल हैं‚ कुछ उम्दा रैस्टोरेन्ट्स भी हैं। तीसरा गेट पीछे को है‚ एसटीसी स्कूल का प्रवेश व निकास। इसके बाहर कई अच्छी सभ्रान्त बस्तियां हैं और थोड़ा बाहर निकल कर‚ थोड़ा रोड चढ़ कर चौराहे के पार मेडिकल कॉलेज है। बीच की सड़कें यहां–वहां से गर्ल्स हॉस्टल्स से जुड़ी हुई हैं।
लेकिन रेजीडेंसी सीनियर सैकेण्ड्री गर्ल्स स्कूल के खेल के मैदान के पार‚ जिधर आदिवासी हॉस्टल है‚ उधर से बाहर निकलने का गेट नहीं है… न पुलिस चौकी… न शहर को जोड़ती चहल–पहल से भरी सड़कें… न कॉलोनियां… जैसा कि पहले मैंने कहा वह उजाड़ कोना है… उसके पार भी शहर की मध्यमवर्गीय या गरीब बस्तियां हैं। इस बड़े मैदान के एक कोने में एक कैन्टीन है। यह मैदान हर हॉस्टल‚ कॉलेज स्कूल के ठीक बीचोंबीच है। वैसे यह कैन्टीन रेजिडेन्सी सीनियर सैकेण्ड्री गर्ल्स स्कूल का है।
कन्या महाविद्यालय का भी अपना अलग कैन्टीन है। लेकिन इस कैन्टीन वाले के समोसे बढ़िया हैं और चाय सस्ती तो इस वजह से यहां गंगा–जमुनी मिलन रहता है लड़कियों का। यहां हरी ट्यूनिक पहने सीनियर सैकेण्ड्री गर्ल्स स्कूल की लड़कियां तो घिरी होती ही हैं। गुलाबी चैक का कुरता और सफेद सलवार–चुन्नी पहने कन्या महाविद्यालय की लड़कियां भी समोसों–चाय पर टूटी रहती हैं। सफेद एप्रन पहने एक दो पीजी डॉक्टर भी कभी खड़ी दिख जाती हैं। एसटीसी स्कूल की नीली साड़ी वाली छात्राएं भी दिख जाती हैं। कभी–कभी बाउण्ड्री फांद कर आई दो चार धाकड़ आदिवासी लड़कियां भी दिख जाती हैं‚ चाव से समोसे खाती‚ जिनके चेहरों व हाथों पर गुदने गुदे होते हैं‚ गहरा चमकीला काला रंग‚ अनगढ़ नक्श!
अरे! …और यह मैं हूँ‚ यहाँ एन्टीगोनम की बेल के गुलाबी फूल तोड़ती! हाँ! यहीं तो कन्या महाविद्यालय के हॉस्टल में रहती हूँ मैं।
मेरी नींद खुल गई है — वह माहौल और वे दिन कल की ही की–सी बात तो लगते हैं। मैं ने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन यहीं से तो किया था। मैं चकित हूँ — कैसे वह पूरा का पूरा माहौल सपने में उतर आया?
पर कल रात …क्या मैं कुछ ऐसा ही लिख रही थी… हॉस्टल वगैरह…? हाँ‚ कल रात मैं ने एक कहानी की शुरुआत की थी … कुछ दिन पहले न्यूज़ में देखी हुई एक विवादास्पद घटना पर लिखने की कोशिश कर रही थी — "सर्वोदय विद्यालय के कन्या छात्रावास में दो लड़कियों ने यौनशोषण से त्रस्त होकर आत्महत्या की"
वह शहर‚ वह रेज़ीडेन्सी कैम्पस हू–ब–हू मेरे सपनों में आता रहा… जब तक मैं कहानी लिखती रही…
उस इलाके में अंग्रेजों के लगाये बड़े दुर्लभ पेड़ थे… मोर पंखी के लम्बे–लम्बे पेड़‚ जैकेरेण्डा‚ गुलमोहर‚ अमलतास जाने कौन–कौन से लाल‚ जामुनी‚ पीले‚ नीले फूलों के पेड़। कितने तो फलों के पेड़ थे। आम‚ इमली‚ जामुन‚ अमरूद‚ बेल… फलों के मौसम में लड़कियां उन पर झूली रहती थीं। अंग्रेजों की लगायी एन्टीगोनम की गुलाबी फूलों वाली लतरें तो अब पूरे कैम्पस में खरपतवार की तरह उगती थीं, लेकिन इन पेड़ों का बहुतायत में होना बहुत अच्छा भी नहीं था। कई बार किन्हीं–किन्हीं रास्तों और पुरानी सड़कों पर दिन में भी रात का सा अंधेरा छाया रहता था।
मुझे अर्धजाग्रत अवस्था में वह बात याद आ गई।
बीएससी में एडमिशन के पहले वर्ष और पहले ही महीने की बात है। जूलोजी प्रेक्टीकल में डिसेक्शन के बाद ही लैब में मुझे उलटी हो गई‚ तो हमारी लैक्चरर ने मुझे हॉस्टल जाकर आराम करने को कहा। और… और… मैं शॉर्टकट लेकर जूलोजी डिपार्टमेन्ट के पिछवाड़े से निकल‚ आदिवासी कन्या छात्रावास की पगडण्डी पकड़ हॉस्टल की तरफ मुड़ रही थी कि … मुझे एक अधेड़ आदमी दिखा‚ पेड़ की तरफ मुंह करके लघुशंका से निवृत हो रहा था… मैं चलती रही… हाय! वह ज़िप खोले हुए ही अपने जननांग का प्रदर्शन करता हुआ अचानक सीधा हो गया। मैं बेवकूफ ठिठक कर खड़ी हो गई… मैंने जो देखा… उससे मेरी मितली बढ़ गई और मैं हाथ में पकड़ी प्रेक्टीकल फाइल और पेन्सिल बॉक्स वहीं फेंक कर भागती चली गई। वह अनुभव ऐसे थे कि चाह कर भी मैं किसी से कह नहीं पाई। न वार्डन से शिकायत की‚ न मेट्रन को बताया।
आज सोचती हूँ‚ सीधे पुलिसचौकी क्यों नहीं भागी? हॉस्टल जाकर इतना क्यों रोई? मेडिकल गल्र्स हॉस्टल में रहने वाली अपनी चचेरी बहन के अलावा किसी को क्यों नहीं बताया…उन्होंने भी तो यह कह कर टाल दिया — “अरे‚ कितनी उलटियां करेगी? हम तो रोज़ ही ज़िन्दा और मुर्दों का यही सब देखा करते हैं। ले‚ खा यह गोली और यहीं मेरे कमरे में सो रह। शाम को वार्ड से आकर तुझे हॉस्टल छोड़ दूंगी।
तब मुझे दिन ही कितने हुए थे‚ कॉलेज में एडमिशन लिये हुए?
फिर तो पुराने हो गये थे हम‚ मैं ने सबक सीख लिया था‚ अकेले नहीं आना–जाना है। पहले मैं बहुत धाकड़ थी‚ एनसीसी कैडेट‚ लगता था‚ मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा? पर उस घटना ने‚ उस विकृत प्रदर्शन ने ऊपर से तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा पर अन्दर मन के‚ जाने कहां जाकर एक गन्दगी सी चिपक गई थी‚ जो रगड़–रगड़ कर भी नहीं छूटती थी। वह पहला कटु अनुभव था‚ लड़की होने का! अब तो फर्क ही नहीं पड़ता‚ इन्हीं रास्तों पर कितने शोहदे‚ अधेड़ गन्दी–गन्दी बातें बुदबुदाते चले जाते हैं। हालांकि बात पहुंची थी‚ वार्डन तक–प्रिंसिपल तक‚ पुलिस चौकी तक भी‚ फिर तो दिन में भी एक सिपाही गश्त भी करने लगा था।
जल्दी ही हॉस्टल की छतों पर घूम–घूम कर‚ पढ़ते–पढ़ते‚ मुझे पढ़ने के लिये एक एकान्त और धूप–छांव वाला कोना मिल गया था। बस तभी मुझे पता चला था कि हमारे हॉस्टल के पीछे की विंग की छत से रेजीडेंसी का खेल–मैदान लगा है‚ पीछे से वह आदिवासी हॉस्टल भी दिखता है। यह मेरा प्रिय कोना था‚ एंटीगोनम की लतर से ढंका‚ मोरपंखी के एक विशाल पेड़ की छांव लेता‚ पानी की टंकी के पीछे छिपा यह दुर्लभ स्थान। जहां मैं पढ़ती तो थी ही‚ कभी–कभी नई बहार के उन नये दिवास्वप्नों में खो जाती थी‚ कभी–कभी एक सहज उत्सुकता के तहत मैं अपने प्रिय कोने से पढ़ते–पढ़ते आदिवासी हॉस्टल की गतिविधियां देखा करती थी।
वे लड़कियां कभी कपड़े धोते‚ बाल सुखाते‚ कभी–कभी एक–दूसरे की चोटी गूंथती कोई लोकगीत गाते दिख जाती थीं। मुझे लगता वह हॉस्टल दिन के इतने उजालों में भी एक किस्म के अंधेरों में घिरा रहता है। इस हॉस्टल की लड़कियों के चेहरों की तरह इनकी दीवारें‚ मुंडेरें काली क्यों हैं? यहां कभी क्या कोई पुताई नहीं होती? सरकारी बातें तो इतनी होती हैं। मुफ्त शिक्षा‚ बेहतर सुविधाएं‚ बेहतर अवसर—आदिवासी लड़कियों के लिये आरक्षण का एक बड़ा हिस्सा। फिर भी ये हम से बेहतर क्यों नहीं हैं?
मैं उस कोने से देखती‚ हर उम्र की आदिवासी लड़कियां‚ आठ साल से लेकर अठारह साल तक‚ ये सभी रेजीडेंसी स्कूल में पढ़ती थीं। वे सभी मुझे कभी कपड़े धोती दिखतीं तो‚ कभी बाहर चूल्हे पर चाय बनाती। लेकिन कभी वे हमारी तरह शोर नहीं मचातीं थीं‚ न खेलती थीं। हालांकि उनमें से दो राज्यस्तरीय पुस्कार प्राप्त एथलीट भी थीं। मैंने उन्हें अपने कॉलेज के खेल मैदान में प्रेक्टिस करते देखा था।
एक दिन हमारी हॉस्टल की एक सीनियर‚ सोशयोलॉजी में एमफिल कर रही पद्मा दीदी ने मुझसे पूछा‚ क्या मैं उनके साथ ज़रा आदिवासी छात्रावास तक चलूंगी? मैं ने अपनी उसी पुरानी उत्सुकता के तहत हां कर दिया।
दीवारें पास से उतनी काली नहीं थीं‚ जितनी दूर से दिखती थीं‚ थोड़ी सलेटी थीं। बड़ा सा गेट था‚ जिस पर लिखा हुआ 'शासकीय आदिवासी महिला छात्रावास' धुंधला पड़ गया था। एक टूटी दीवार पर शिलन्यास का अवशेष — वह पत्थर किसी नेता की गौरवगाथा कह रहा था। हम खेल मैदान पार करके‚ मोटे लोहे के खुले गेट के अन्दर हॉस्टल के अहाते में खड़े थे। सूखा‚ झड़बेरी की झाड़ियों‚ जंगली पेड़ों‚ बड़ी–बड़ी सूखी घास से भरा वह अहाता‚ जिसमें जगह–जगह जंगली झबरी पूंछ वाले चूहों के बिल थे। हमें देखते ही उछलकूद मचाते चूहे गड्ढों में घुस गये थे। एकाध दुस्साहसी चूहा… दोनों हाथ गिलहरी की तरह उठाए पीछे के पैरों से खड़ा एक सूखी रोटी खा रहा था। पास ऊंचाई पर टूटी फूटी सीढ़ियों पर चढ़कर एक पंक्ति में कुछ मटमैले कमरे थे। दोपहर ढल रही थी पर एक अलसायापन माहौल पर तारी था। एक अलसाई शान्ति धूप के साथ–साथ मैदान और हॉस्टल की छत पर पसरी थी।
पद्मा दीदी के हाथ में उनके डेज़र्टेशन वर्क के कुछ छपे हुए पर्चे थे‚ यह शायद एक प्रश्नावली थी‚ अजीबोगरीब प्रश्नों वाली। वे हमसे भी कई बार यह सब भरवा चुकी हैं। यहां कोई चौकीदार नहीं था। एक मैट्रननुमा अधेड़ आदिवासी स्त्री एक पेड़ के नीचे चारपाई पर बैठी थी। गले में लटकी चिमटी से दांत खोदती। पास ही बीड़ी का बण्डल पड़ा था। गोल–गोल भेदक आंखें और चपटी नाक और मोटे होंठ। माथे पर गोदने की कई बिन्दियां थीं‚ पर उसने सिन्थेटिक‚ छींट का हरा सलवार कुर्ता पहना था‚ दुपटट चारपाई पर‚ तकिये की जगह सिरहाने गोल–मोल बिछा था। वह हमसे बुरी तरह बोली
" क्या है?"
" मैं रिसर्च कर रही हूँ‚ मुझे यहाँ की लड़कियों से यह पर्चे भरवाने थे।"
" आपने किससे परमिशन ली?"
" किसी से नहीं‚ मैडम‚ ये सादा पर्चे हैं‚ सवालों के लड़कियों से भरवाने हैं। जैसे उनकी उम्र‚ माता—पिता क्या करते हैं‚ गांव‚ क्या पढ़ती हैं?"
" आपसे मतलब! हमारी लड़कियां क्या पढ़ रहा है? फिर आना। भागो भागो।"
तब तक लड़कियां जो पढ़ तो कतई नहीं रही थीं, कमरों से बाहर निकल आईं। मैंने उन्हें ध्यान से देखा‚ छोटी–छोटी लड़कियां … जंगली मैना सी…मानो यहां आकर वह स्वच्छन्दता भूल गई हों‚ जबरन एक उदासीनता तह जमा कर चेहरे पर पोते हुए थीं, पर कहीं भीतर एक मिट्ठू सा कौतुहल आंखों की कोटरों में से झांक रहा था। बड़ी लड़कियां एक तटस्थता के साथ हमारे कपड़ों और हमारे चेहरों को आंक रही थीं। वे गलियारे के चूना उखड़े खम्भों से सटी खड़ी थीं। खम्भे ही नहीं एक–दूसरे से भी सटी। लगभग एक से कटाव के अनगढ़ सांवले चेहरे। एकाध थोड़ा गोरा चेहरा‚ और बाल भूरे भूरे। तरह–तरह के गोदने। सभी के नाक कान छिदे हुए पर आदिवासी गहने नदारद थे। वे सभी अलग–अलग रंगों के मगर लगभग एक सी प्रिन्ट के सूती कपड़े पहने थीं‚ उम्र के हिसाब से। बच्चियों ने फ्रॉक‚ लड़कियों ने सलवार–कुर्ते। शायद खाना–फीस‚ किताबों के साथ कपड़े भी उन्हें सरकारी अनुदान से मिलते हैं।
" ए‚ सुना नहीं क्या?" मैट्रन फिर गुर्राई।
" अरे! आप समझ ही नहीं रहे हो… हम बस सर्वे के लिये आये हैं‚ भील जनजाति की लड़कियों पर। देखो अगर तुमने मुझे अन्दर नहीं जाने दिया तो मुझे क्षेत्रीय जनजाति विभाग के दफ्तर जाकर शिकायत करनी पड़ेगी। यह सरकारी सर्वे है। मैं वहीं से पूछ कर ये पर्चे लेकर आई हूँ।"
मैट्रन पद्मा दीदी के छद्म रौब से डर गई।
तभी उन बड़ी लड़कियों में से एक सीधे दालान में उतर आई‚ "क्या बात है बइण जी?" पास से देखकर मैं पहचान गई यह वही एथलीट लड़की है। लम्बा हरा कुर्ता‚ बेढंगी सिली‚ पीली हो आई सफेद सलवार पहने। अनगढ़ नाक में मोटी गुलाबी नग की लौंग‚ गहरा काला रंग‚ बड़ी आंखें… मोटे होंठ… जिन्हें आज आप 'क्यूपिड की बो' की उपमा दे सकते हैं। लम्बा‚ दुरूस्त मांसपेशियों से कसा–कसा बदन।
"तू अन्दर जा…।"
" आने दो इनको‚ मैं जानती हूं इन दीदी को।" उसने मेरी तरफ उंगली कर दी।
"ठीक है‚ बेनुड़ी तेरी जिम्मेदारी।" मैट्रन पर उसके भी रौब का असर हुआ। वह चुपचाप चारपाई पर लेट कर बीड़ी पीने लगी।
पद्मा दीदी ने रास्ते में आदिवासी लोगों के बारे में बहुत कुछ बताया था कि इनमें ज़्यादातर लड़कियां भील जनजाति की हैं। सही अर्थों में वन कन्याएं। सर्वे का क्वेश्चनायर भरवाते में पता चला कि कुछेक लड़कियां जो थोड़े गोरे रंग की थीं‚ वे कंजर जनजाति की थीं‚ ये कंजर कन्याएं ज़रा फैशनेबल सी थीं। सुर्ख नेलपॉलिश लगाये‚ काजल लदी आंखें और उनमें एक कटाक्ष‚ तीखे होंठ जिनमें एक जन्मजात विलास!
एक लड़की गाड़ियालोहार जनजाति की भी थी। गाड़ियालोहार वही लोग हैं‚ जिन्होंने महाराणा प्रताप का युद्ध में साथ दिया था, अपनी कृषिभूमि दान कर कसम खाई थी कि वे अब कभी घर बना कर नहीं रहेंगे‚ गाड़ियों में घर बनाएंगे और प्रदेशभर में घूमेंगे। भील‚ कंजर‚ गाड़ियालोहार कुल मिलाकर दस बारह आदिवासी लड़कियां। आधे कमरे लगभग खाली ही थे। पद्मा दीदी को लड़कियों ने घेर लिया था। वे स्वयं ही पूछ–पूछ कर प्रश्नावली भर रही थीं‚ और खरीद कर लाया केक बांट रही थीं।
मैं एक बैंच पर बैठ कर यहां–वहां ताक रही थी। इस छात्रावास के कमरे क्या थे‚ दड़बे ही थे। न जाने कब से पुताई नहीं हुई थी। मैं ने बैंच पर बैठे–बैठे कमरों में झांका‚ कमोबेश हर कमरे का एक ही सा परिदृश्य—अलमारियां नदारद‚ बस कुछ ताखें थीं जिन पर आदिवासी लड़कियों ने अपने पीतल–कांसे के बर्तन जमा रखे थे। या कंघा और शीशा। कमरे के बीच में चारपाई की मूंज की रस्सी बंधी थी जिस पर कपड़े‚ स्कूल की यूनिफॉर्म बेतरतीबी से टंगे थे। टेबल नहीं थी‚ डेस्क थीं उन पर किताबें थीं। प्रकाश के लिये मकड़ी के जालों से ढका धूमिल बल्ब‚ कांच की खिड़की बन्द थी उस पर मोटा काला कागज चिपका था। कैसे पढ़ती होंगी इतनी कम रोशनी में?
जिन लड़कियों ने प्रश्नावली भर दी थी वे कुतुहलवश मेरे पास भी आ गयीं। उनमें से एक एथलीट भी थी।
“ आप मीरा गर्ल्स कॉलेज में हो न?”
“ हाँ।”
“ आपको बास्केट बॉल खेलते हुए देखा था।”
“ हाँ, मैं ने भी तुम्हें देखा था। क्या तुम यहीं रैजिडेंसी स्कूल में पढ़ती हो?”
“हाँ।”
“भर दिया पर्चा?”
“हाँ, पर्चा तो भर दिया। पर म्हैं सोच्यो पर्चा मां पूछोला कि…” मेरे चेहरे पर राजस्थानी न समझ पाने की उलझन देख कर वह हिन्दी में बोलने लगी, “ हम कैसे यहां रहते हैं, क्या खाते हैं? हमें मिलने वाली छात्रवृत्ति को कौन खा जाता है। पण पर्चे में तो होर ई बातां हैं। हमारी जात, रीत–रिवाज, एक से ज्यादा सादी, औरतों की खरीद–बेच के बारे में प्रस्न हैं।” पता नहीं उसकी बात में तंज था, कड़वाहट थी या सरलता! कुछ लड़कियां आपस में आधी हिन्दी–आधी बागड़ी राजस्थान के बागड़ क्षेत्र डूंगरपुर–बांसवाड़ा की बोली हृ में बात कर रही थीं।
“ वो बात ये है कि वो जो दीदी हैं, ये ही विषय पढ़ती हैं, जिसमें जातियां और उनके रीति–रिवाज के बारे में होता है, तुम भी तो पढ़ते होगे ना सामाजिक विज्ञान में।” मैंने बेजा सफाई दी, उसका असंतोष और उमड़ पड़ा।
“ पैले भी कितनेक संस्थावाले, एनजीओ की औरतें आईं, मैट्रन और इंचारज ने झूठ–झूठ बता के फुटा दिया।”
“तुम्हारा नाम क्या है?”
“बेनु”
“बेनु, कुछ समस्या है क्या…?” उसके असंतोष ने मेरी उत्सुकता बढ़ा दी थी।
“समस्या क्या एक है, दीदी? शश्श…मेट्रन आ री है। पढ़ाई की बात करो।
“किस कक्षा में पढ़ती हो?…”
पदमा दीदी का काम पूरा हो चुका था। छोटी लड़कियों को उन्होंने टॉफियां पकड़ाईं और हम वापस आ गए। लेकिन बेनु के साथ सिलसिला बना रहा तब तक जब तक कि... वह अचानक गायब नहीं हो गई। एक दिन अचानक अखबार की सुर्खियों में आकर उसने मुझे चौंका दिया।
गायब होने से थोड़ा पहले वह अकसर मुझसे हॉस्टल मिलने आया करती थी। या फिर हम मिलते थे, खेल के मैदानों में। कैंटीन में। पेड़ों से छायादार रास्तों में।
“मनु जीजी, कल खेलने नहीं आईं आप?”
“नहीं, मेरा ज़ूलॉजी का प्रेक्टिकल था।”
“मैं स्टेट लेवल पर सलेक्ट हो गयी।”
“अच्छा! यह अच्छी खबर है। चाय पिएगी, चलें कैन्टीन?”
“जयपुर जाना पड़ेगा।”
“कब?”
“अगले महीने ही। लेकिन वो कमीनी मेट्रन लिखत में परेमिसन नहीं दे रही। इंचारज भी भग गया है।”
“क्यों?”
“कुत्ती रांड, कहती है कि पैले मां–बाप से दसखत लेकर के आ। डूंगरपुर से भी आगे सालमगढ़ तहसील के पास हमारा गांव है। आणे–जाणे में तीन दिन तो लगेंगे ही… दीदी पैसे हों तो…”
“पैसे! बेनु पहले तू मेरे पहले के सौ रुपए लौटा।”
“पैले के दो महीने की छातरवर्ती इंचारज ने अटका रखी है। पांचसौ पूरे तो कभी देता ही नहीं खा–पीके दो सौ टिकाता है, फेर भी चारसौ बनते हैं, मिलते ही दे दूंगी।”
“ऐसा क्यों करता है?”
“करता है उसके बाप का राज है, नहीं करेगा अगर उसके बिस्तर पे कपड़े काढ़ के…रांड रा…”
“क्या बकवास करती रहती है बेनु?”
“बताया नहीं आपको पैले… छोटकी चिरमी… दस्स बरस की… इंचारज के पास फीस के पैसे लेने गई और पूरी चड्डी लाल।…”
“मुझे मत बताया कर यह सब, जाकर पुलिस को बता…।” मैं घबरा गई थी।
“पुलिस? वो हमारे यहां की दोनों कंजड़िनें हैं न, उनको ले जाके इंचारज पुलिस को खुस रखता है।”
“मैट्रन?”
“वो रण्डी तो पैसे के बदले अपनी बेटी बेच दे।”
माना मैं उस साल अठारह की हुई थी और कहने भर को वयस्कों में शुमार हो गई थी, मगर ये ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ने वाली स्कूल की लड़की क्या बातें कर रही थी? मेरा मन घबरा गया था उन बातों से। मैं ने उसे पैसे तो नहीं दिए बल्कि उससे कतराना भी शुरु कर दिया। पद्मा दीदी ने डरा अलग दिया… “मनस्वी तू चुप बैठ। उससे बात मत किया कर। वो खुद कम नहीं है। मैं उसे उसके कोच के साथ घूमते देखा है। वह कोई बच्ची नहीं है। उसकी शादी भी हो चुकी है पर सब छोड़छाड़ के पढ़ने चली आई थी।”
“गलत तो नहीं किया दीदी… कितनी आदिवासी लड़कियां…”
“बस, बताया न उससे मत मिला कर। अपने पैसे जल्दी ही वापस ले लेना।”
“पर दीदी वो छोटी उम्र की भील लड़कियां?''
"ऐसी बातें छिपती हैं क्या? एक दिन खुलेंगी। फिर हम क्या कर सकते हैं? हम यहां पढ़ने आये हैं। इससे सालों पहले से आदिवासी छात्रावास यहां है। यह सब तो…" उन्होंने मुझे समझा कर भगा दिया था। बेनु मुझसे फिर नहीं मिली। शायद वह अपनी स्टेट लेवल पर होने वाले टूर्नामेन्ट की तैयारियों में व्यस्त थी।
आदिवासी कन्या छात्रावास की ऐसी बातें मैं ने कई बार बेनु के मुंह से सुनीं थीं… इन सब बातों के बाद मैं ने उससे मिलना तो बन्द कर दिया था‚ लेकिन बहुत विचलित रही मैं। भीरू थी मैं? नहीं‚ उम्र की विवशता थी‚ मैं खुद बीएससी ही तो कर रही थी। किस से जाकर क्या कहती? …कौन सुनता तब मेरी? बेनु की ही किसी ने नहीं सुनी तब… अब बात अलग है…
इस कहानी के जन्म के दौरान मैं ने फिर सपना देखा —
मैं बेखबर अपने मनपसन्द कोने में बैठ कर अगले दिन होने वाली कैमिस्ट्री के पेपर की तैयारी कर रही हूँ‚ सर्दियों के दिन थे सुबह की मीठी धूप अचानक कड़वी हो गई है। आदिवासी छात्रावास में शोर गूंजा। चीख–चिल्लाहटें‚ छोटी लड़कियों का रोना… दस पन्द्रह मिनट मेंं पुलिस आ गई है। मुझे छत पर से कुछ नहीं दिखा‚ मैं कुछ समझ नहीं सकी… पर उन छोटी लडकियों की घुटती हुई चीख इतनी दिल दहला देने वाली थी कि मैं घबरा कर नीचे आई हूं। कमरे में जाकर मैं कपड़े बदल कर आदिवासी छात्रावास दौड़ जाती… अगर पद्मा दीदी ने वहीं हाथ पकड़ कर घसीट कर मुझे अपने कमरे में बन्द न कर लिया होता।
"बेवकूफ है क्या?"
"हुआ क्या है?"
"सुनेगी? सुनना चाहती है न? सुन और फिर जा… आदिवासी हॉस्टल में दो लड़कियों ने आत्महत्या की है।" वे डांट रही थीं।
"……" मैं कुछ समझ ही नहीं पाई।
"अब मैंने तुझे देखा ना‚ बेनु के आसपास तो मुझे तेरे पेरेन्ट्स को फोन करना पड़ेगा कि आपकी बेटी किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली है। अभी तू चुपचाप यहां से जाकर अपनी कज़िन सुनयना के पास मेडिकल हॉस्टल चली जा‚ वहीं पढ़ कर एग्ज़ाम देना।"
नींद फिर आई नहीं … मैं कैसे सोती! सपना था? पूरी रात उन्हीं रास्तों में भटकी हूं। उदयपुर का रेजीडेंसी इलाका… जहां की शै‚ हर दरख्त‚ हर बेल–बूटा‚ टूटी दीवारें‚ कच्चे–पक्के रास्ते बहुत जाने पहचाने थे। उन लोगों के बीच पहुंच गई हूं जिनके साथ वह अहम् वक्त सात साल का गुज़रा था‚ शुरू का चहकते–महकते। बीच का डरते–सहमते। बाद का एक ऊब और तटस्थता के साथ।
पर यह बात तो सच थी‚ बीएससी फाइनल ईयर में मेरे ऑर्गेनिक कैमेस्ट्री के पेपर के दिन कुछ तो हुआ था। पर क्या? एक ऑटो वाले का मर्डर! हमारे ही कैम्पस में! मेरा आर्गेनिक कैमेस्ट्री का पेपर बिगड़ गया था। गनीमत थी कि वह आखिरी था। उसके बाद लम्बा गैप फिर प्रेक्टीकल एग्ज़ाम्स थे। पर जब पेपर देकर आई तो पूरा हॉस्टल न्यूज़पेपर्स की टेबल पर जमा था। सब सकते में थे। क्या यह कैम्पस अब सुरक्षित रह गया था‚ गर्ल्स हॉस्टल्स के लिये? बीएससी के बाद भी यहीं से एमएससी करना विवशता थी और मैंने की… उसी डर और अविश्वास के साथ।
आज जिस तटस्थता से कह रही हूँ‚ इस तटस्थता की अवस्था तक पहुंचना क्या आसान था?
इन्सोम्निया टर्म तब मैं जानती नहीं थी‚ न ही तब यह टर्म महिलाओं में आम थी आज की तरह। तब नींद न आने‚ डरने की बात पर लड़कियों को उनके माता–पिता मनोचिकित्सक के पास नहीं ले जाया करते थे। लेकिन मुझ पर इससे भी कुछ गंभीर गुज़रा था जिसके निशान अब तक अंतस पर गहरें हैं। शायद यही वजह है कि — वह रैजिडेंसी कैम्पस हू–ब–हू यूं मेरे सपनों में आ गया‚ इतने सालों बाद!
मैं उस बेनु से नहीं मिली फिर पता नहीं वह कहां चली गई? बहुत दिनों बाद जिससे मिली तो वह बेनु थोड़े ही न थी… वह तो बनमाला… थी।
लेकिन कल रात अचानक वही बेनु सपने में आकर उस कैन्टीन की बैंच पर बैठ कर मुझसे क्या कह रही थी? ठीक से याद नहीं आ रहा था… कोई कड़ी टूटकर हाथों से छूट–छूट जा रही थी। इन्होंने मुझे अचानक जो जगा दिया था…" अरे! मनु तुम कैसी आवाजें निकाल रही हो?" और वह कड़ी वहीं टूट गई… मैं किस हॉस्टल की टूटी दीवार की बात कह रही थी?
ओह! याद आ गया…
सपने में — वही कैन्टीन‚ टीन की छत वाला… सामने घास का मैदान‚ बगल में एक गड्ढा जिसके आस–पास गुलाबी एन्टीगोनम के फूल खिले थे। मैं और बेनु लकड़ी की संकरी बैंच पर बैठे हैं खुले आसमान के नीचे। सर के ऊपर एक बादल का टुकड़ा तैर रहा था। मैं उसी युनिफॉर्म में…गुलाबी… सफेद… नहीं… सफेद स्कर्ट था‚ हाथ में बास्केटबॉल थी। उसने क्या पहना था? दिखा नहीं… चेहरा भी स्प्ष्ट नहीं। गोदना याद है… तोता–मैना वाला हाथ की संवलाई त्वचा पर नीला गाढ़ा गोदना।
मैंने उससे चीख कर पूछा था— " कहां जा कर मर गई थी कम्बख्त‚ कितनी चिन्ता हुई तेरी! जयपुर से कब लौटी?" फूट–फूट कर रो दी हूँ मैं पूछते–पूछते।
"कहाँ? कहां गई जैपुर? जाने नईं दिया न कुत्ते इंचारज ने।"
"………।"
"कोच सर ने कहा भी उससे कि वो सिकायत करेंगे इंचारज की … जनजाती विभाग में‚ बड़े साब से एक प्रतिभासाली भील छात्रा को तुम खुद ही आगे नहीं आणे देते।"
"……"
"कोच सर ने एप्लीकेसन लिखवाई‚ मैंने सब कुछ लिख दिया था उसमें। छोटी लड़कियों के साथ छेड़खानी‚ पुलिस चौकी वालों का कंजरियों के कमरे में आना… मैट्रन भी कुत्ती कंजर जाती की थी न। भीलनियों की जात भले ही छोटी हो‚ आन बड़ी होती है‚ इज्जत भी।"
“……"
" वो अपलीकेसण मेरे कन्ने थी। पेटी–बकस में। मैट्रन ने पीछे से निकाल ली‚ ताला तोड़ के पेटी का। उसी दिन कोच सर और मैं जाते… जनजाती के दफ्तर… क्योंकि मेरा जैपुर जाना बहुत जरूरी था। स्टेट के बाद‚ नेसनल फिर इन्टरनेसनल… कोच सर कहते हैं कि तू बहुत ऊपर जाएगी बेनु।"
"……"
"कहां जा सकी। आते ही इंचारज और मैट्रन ने खूब मारा… हाथ छुड़ा के रात के अंधेरे में भागी थी मैं … वो हॉस्टल के पीछे की टूटी दीवार… से कूद के… शहर के उस तरफ… माथे पे चोट लगी…लहू ही लहू … पर पकड़ लिया…उस हड़क्ये कुत्ते ने‚ दोनों ने मिल कर गला टीप दिया। फिर रस्सी लटका दी गले में…"
"……"
"कौन? मुन्नी? उसे क्या हुआ? न मुझे नहीं पता। वो तो घर गई हुई थी। ना! ना! वो मेरे साथ नहीं थी। उसे भी मार डाला क्या …?" वह चीख रही है मुझे झिंझोड़ते हुए।
मैं फिर उठ बैठी हूँ पसीने में तर–ब–तर। कौन मुन्नी? कौन बेनु? यह कैसा सपना था?
"क्या हुआ मनु?" इन्होंने मुझे झिंझोड़ कर पूछा।
"……।" मैं पसीने–पसीने बुत बने‚ रजाई उघाड़े बैठी कांप रही थी।
"वो हॉस्टल की टूटी दीवार…।"
"मनु! सपना देखा?"
"… हां शायद पर… ऐसा लगा सच ही था।"
"डर गई हो सो जाओ।" वे करवट बदल कर सो गये।
मैं नींद में अपना आप टटोल रही हूँ। अजीब सी नींद में स्वयं से पूछ रही हूँ — कौन थी यह बेनु? कहीं 'बनमाला' तो नहीं? अरे! अभी पिछले महीने मेरे जन्मदिन पर तो फोन आया था उसका।
यह कहानी तो उसकी ही कहानी है‚ उसके सिर का वह निशान और उसका इतिहास …उसीने तो बताया था। पर उसने तो कभी आत्महत्या नहीं की। वह अखबार की सुर्खियों में ज़रूर आई थी। लेकिन इस तरह — 'पहली भील आदिवासी लड़की आर। पी। एस। बनी।' मैंने उसे बधाई दी थी‚ पता ढूंढ कर… तब से वह मुझसे फोन पर सम्पर्क रखती आई है। दो बार वह घर भी आई है। उसने कोच से विवाह कर लिया था‚ जयपुर जाकर। उसी ने‚ उसके कोच देवराजसिंह मीणा ने उसे आगे पढ़ाया और इस गरिमामय पड़ाव तक उसे ले आया।
मेरे हाथ–पैर बरफ हो रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है। यह सब क्या है? मेरी समाचार वाली कहानी बनमाला से क्यों जा जुड़ी है? वह तो ज़िन्दा है। अपने उसी जांबाज़ व्यक्तित्व के साथ। एक पुलिस अधिकारी के ज़िम्मेदार पद पर बैठ न जाने ऐसे कितने साधुओं‚ नारीनिकेतनों‚ छात्रावासों के गंदले गुदड़ों के बखिया उधेड़े हैं और वहां के निकृष्ट कर्मचारियों को पिस्सू—सा निकाल फेंका है।
पूरे सप्ताह कहानी लिखने के दौरान मुझे न जाने क्या–क्या याद आता रहा है‚ और मैं अपनी मूल कहानी से भटककर उदयपुर‚ रेजीडेंसी के उस विस्मृत इलाके में घूमती रही हूँ। कुछ सच‚ कुछ स्वप्न … मुझे नहीं पता यह कहानी स्वयं अपने आपको और मुझे कहां ले आयी है? पर गनीमत है‚ पूरी तो हुई‚ अब कहीं जाकर मेरा मन संभला है।
बस पेन और डायरी को रख दिया है‚ भीतर… अलमारी में …! अब एक–दो महीने कोई कहानी नहीं लिखूंगी। उफ! कम से कम किसी अखबार की छपी दारुण खबर को प्लॉट बना कर तो कभी नहीं‚ ये खबरें जब आपके अतीत से कहीं छूकर गुज़रती हैं तो अवचेतन पर जाकर‚ नाना प्रकार की रासायनिक क्रियाओं से गुज़र कर‚ सपनों के धरातल पर प्रेसीपिटेट (अवक्षेपित) होती हैं।