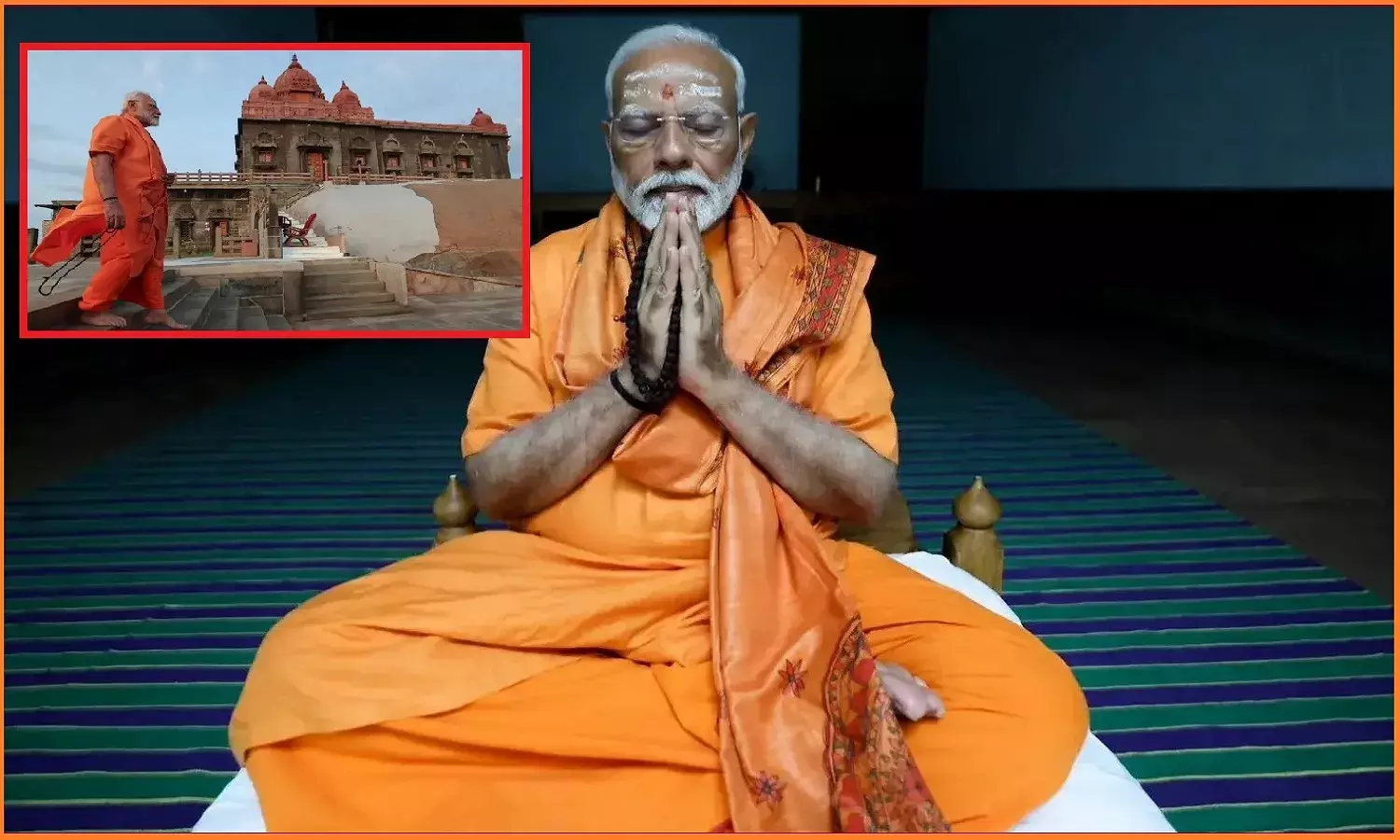आफ्सपा जैसे काले कानून के रहते पूर्वोत्तर नहीं बन सकता 'इकॉनोमिक हब'

दिनकर कुमार का विश्लेषण
असम सरकार ने राज्य में सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम, 1958 (अफस्पा) को 28 अगस्त से छह और महीनों के लिए बढ़ा दिया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि पूर्वोत्तर में सुरक्षा बलों पर हाल के विद्रोही हमलों और असम के विभिन्न क्षेत्रों से अवैध हथियारों और गोला-बारूद की बरामदगी के कारण राज्य को "अशांत क्षेत्र" घोषित किया गया है। भले ही असम में इसकी अवधि बढ़ाई गई है लेकिन समूचे पूर्वोत्तर राज्यों में इसकी प्रासंगिकता घटती गई है।
सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (अफस्पा) एक 'अपवाद' के तौर पर 1958 से पिछले छह दशकों से उत्तर पूर्व भारत को परिभाषित करता रहा है। अब यह कानून धीरे-धीरे इस क्षेत्र की बदलती धारणाओं के साथ अपनी प्रासंगिकता खो रहा है। अब तक मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम सहित तीन राज्यों से इसे निरस्त कर दिया गया है। यह मूल रूप से औपनिवेशिक समय से एक अवशेष था, जो 1942 में वजूद में आया था।
अफस्पा मुक्त उत्तर-पूर्व एक वास्तविकता बन रहा है क्योंकि क्षेत्र खुद को 'आर्थिक हब' बनने के लिए बदल रहा है, जबकि हिंसक उग्रवाद धीरे-धीरे दूर हो रहा है। आजादी के बाद से इस क्षेत्र में उग्रवाद का सिलसिला चलता रहा था और उग्रवाद से निपटने के लिए अफस्पा का इस्तेमाल किया गया।
विवादित कानून अफस्पा को असम और मणिपुर में 11 सितंबर 1958 को लागू किया गया और 1972 में संशोधित किया गया था ताकि पूर्वोत्तर के अन्य सभी राज्यों में इसे विस्तारित किया जा सके जो पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, 1971 के तहत असम से बाहर थे। जब अलगाववादी आंदोलनों ने भारत के साथ औपनिवेशिक काल के बाद के एकीकरण का विरोध किया, तो पूरे क्षेत्र को 'अशांत' घोषित किया गया।
अलगाववादी आंदोलनों ने कई दशकों तक भारतीय प्रशासन को एक गंभीर चुनौती दी। समय गुजरने के साथ इन आंदोलनों में से अधिकांश ने, जो क्षेत्र में लोगों की क्षेत्रीयता और जातीयता के आधार पर एक स्वतंत्र पहचान की चिंता से आरंभ हुए थे, अपना प्रभाव खो दिया है।
अफस्पा के लागू होते ही ढेर सारे प्रतिबन्ध लागू हो जाते हैं जैसे कि पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर इकट्ठा होने पर प्रतिबंध, आग्नेयास्त्रों को अपने पास रखने पर प्रतिबंध और इसी प्रकार के अन्य प्रतिबन्ध लागू हो जाते हैं। अफस्पा सेना को बल प्रयोग करने की भी छूट देता है जिसमें उचित तौर पर चेतावनी देने के बाद गोली मारने और "पर्याप्त संदेह" के आधार पर गिरफ्तारी की अनुमति देता है और अन्य प्रावधानों के साथ ही साथ यदि ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति नियम-कानून तोड़ रहा है तो बिना किसी वारंट के उसके स्थान की तलाशी लेने जैसी कार्यवाही करने की इजाजत देता है। उपरोक्त सभी चीजें सेना अफस्पा के तहत करती है और जो सेना के खिलाफ किसी भी प्रकार के क़ानूनी कार्यवाही के लिए कोई प्रावधान नहीं छोड़ते।
यह ब्रिटिश हुकूमत थी जिसने पहले पहल आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स को एक अध्यादेश के रूप में 1942 में लागू करने का काम किया था, ताकि महात्मा गांधी द्वारा छेड़े गए भारत छोड़ो आंदोलन को किसी भी तरह से कुचला जा सके। देश विभाजन के समय भी आंतरिक सुरक्षा से निपटने के लिए 1947 में केंद्र सरकार ने अफस्पा कानून लागू किया था। इसी तरह 1953 में, असम सरकार ने नगा हिल्स में नगा नेशनल काउंसिल (एनएनसी) का मुकाबला करने के लिए अफस्पा का इस्तेमाल असम मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर (स्वायत्त जिला) एक्ट के तहत किया था, जो भारत से आज़ादी की माँग कर रहे थे।
स्थिति को काबू में नहीं किया जा सका और मार्च 1956 में नगा नेशनलिस्ट काउंसिल (एनएनसी) ने एक समानान्तर सरकार खड़ी कर डाली, जिसे नगालैंड की संघीय सरकार (फ़ेडरल गवर्नमेंट ऑफ़ नगालैंड) का नाम दिया गया। इससे निपटने के लिए, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स आर्डिनेंस 1958 को अस्तित्व में लाया गया था।
लगातार बातचीत के जरिये 1949 और 2015 के बीच नगा विद्रोहियों के साथ लगभग 14 शांति समझौते हुए हैं, और जल्द ही इस मसले को हल कर लेने का दावा किया जा रहा है। इस लंबी कठिन यात्रा में अफस्पा पूर्वोत्तर में सबसे भयानक और विवादास्पद कानून बना रहा, जिसके तहत भारतीय सेना को 'कानून और व्यवस्था' के नाम पर किसी को भी गोली मारने, गिरफ्तार करने और तलाशी लेने की असीमित शक्ति दी गई है।
इसने उत्तर-पूर्व में एक गहरा विभाजन और संकट का माहौल पैदा कर दिया। नागरिकों ने इसे निरस्त करने और समस्या के राजनीतिक समाधान के लिए लगातार आवाज़ बुलंद की है। मणिपुर की इरोम शर्मिला वर्ष 2000 से सोलह लंबे वर्षों तक विरोध का एक प्रतीक बन गईं। अपनी युवावस्था में उन्होंने इस तरह के कानून के खिलाफ लड़ने और मणिपुर में अपने साथी नागरिकों के लिए सामान्य स्थिति बहाल करने का संकल्प लिया था। उसकी युवावस्था और ऊर्जा का बलिदान हो चुका है, लेकिन उनका लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया।
(दिनकर कुमार पिछले तीस वर्षों से पूर्वोत्तर की राजनैतिक मसलों की रिपोर्टिंग करते रहे हैं।)